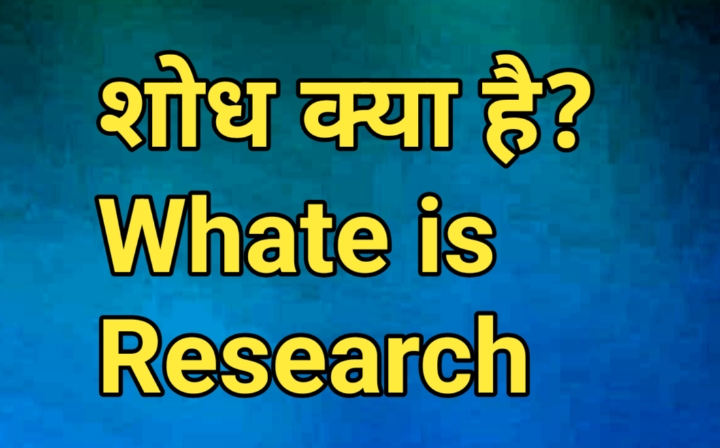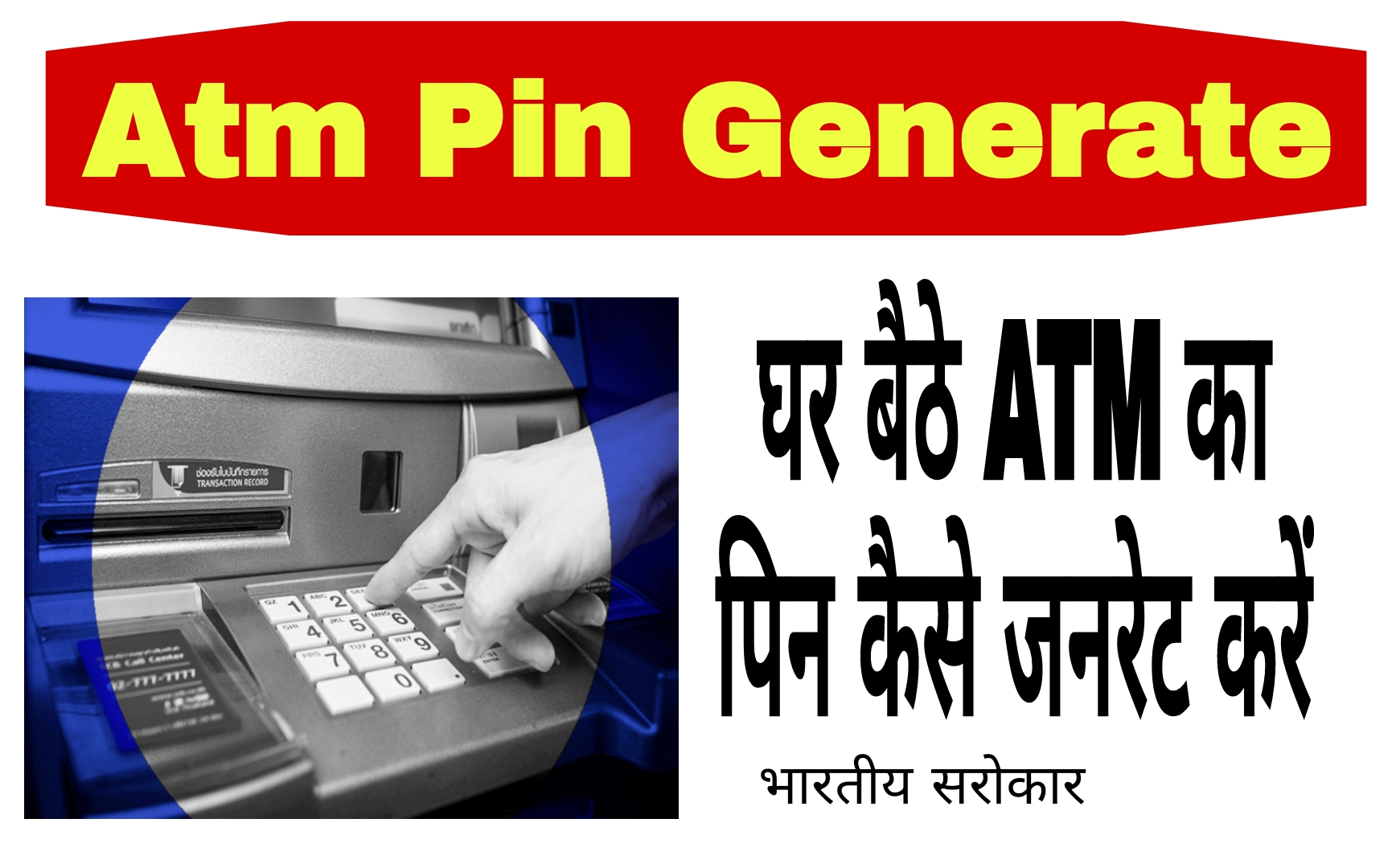दुर्खीम का कहना है कि ‘सामाजिक तथ्य’ को वस्तुओं के समान समझना चाहिए। दुर्खीम वस्तु शब्द का चार अलग-अलग अर्थों में प्रयोग किया है जो इस प्रकार है-
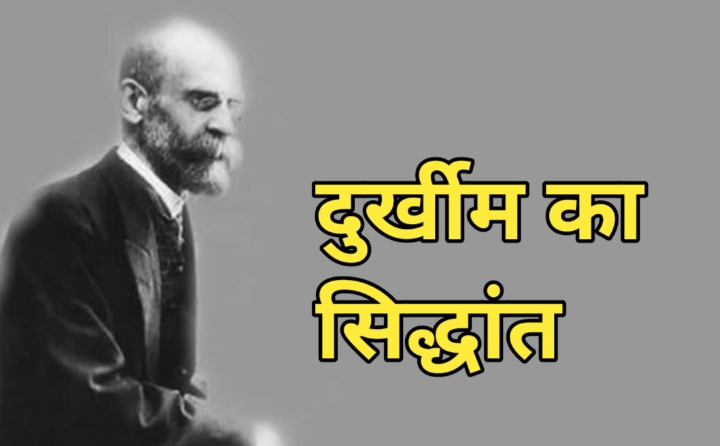
1. सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते है जिन्हें बाहरी तौर पर देखा जा सकता है।
2. सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिन्हें केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है।
3. सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जो केवल अनुभव पर बिल्कुल ही निर्भर नहीं है।
4. सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसको केवल बाहरीतौर पर देखकर ही जाना जा सकता है।
इस दृष्टिकोण से सामाजिक तथ्य कोई स्थिर धारणा नहीं बल्कि गतिशील धारणा है।
सामाजिक तथ्य की परिभाषा :- दुर्खीम के अनुसार ” सामाजिक तथ्य व्यवहार (विचार) अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप में संभव है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने का बाध्य करता है।” दुर्खीम ने आगे लिखा है कि “सामाजिक तथ्यों का संबंध कार्य करने विचार करने और अनुभव करने के उन सभी तरीको से है जो व्यक्ति के लिए बाह्य होते है जो अपनी दबाव शक्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारो को नियंत्रित करते है।”
सामाजिक तथ्य की विशेषता :- दुर्खीम सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझने के लिए दो शब्दों का बाह्यता तथा बाध्यता प्रयोग किया है-
1. बाह्यता (Exteriority)– सामाजिक तथ्यों में बाह्यता का गुण निहित होता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथ्यों का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। जब कोई सामाजिक तथ्य विकसित हो जाता है तो फिर उसका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतन्त्र हो जाता है। दुर्खीम का कहना है कि सामाजिक तथ्यों का निर्माण सामूहिक चेतना से होता है। यह सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से बिल्कुल अलग होती है।
2. बाध्यता (Constraint)- सामाजिक तथ्यों में वाध्यता का गुण होता है। यह व्यक्ति को एक विशेष ढंग से विचारकरने और व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। इनका व्यक्ति पर इतना अधिक दबाव होता है कि वह अपनी इच्छा या अनिच्छा से उनके विरूद्ध नहीं जा सकता। सामाजिक तथ्यों में बाध्यता का गुण इस बात से भी स्पष्ट होता है कि यह प्रत्येक दशा में व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते है। लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छानुसार इन्हें नहीं बदल सकता। दुर्खीम ने इसका कारण स्पष्ट करते हुए बताया है. कि सामूहिक चेतना वैयक्तिक चेतना से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है अतः सामाजिक तथ्यों में बाध्यता का गुण आ जाना बहुत स्वाभाविक है।
सामान्य और व्याधिकीय तथ्य (Normal and Pathological Social Facts) दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए दो मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया है-
1. सामान्य सामाजिक तथ्य:- दुर्खीम के अनुसार सामान्य सामाजिक तथ्य वे है जो एक विशेष अवधि में किसी समाज में सामान्य दर से पाये जाते है।
2. व्याधिकीय सामाजिक तथ्य :- व्याधिकीय सामाजिक तथ्य का अर्थ उन दशाओं से है जो समाज के लिए हानिकारक होती है।
सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों की प्रकृति को दुर्खीम ने एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है-दुखींम का कहना है कि ‘अपराध ‘समाज के लिए हानिकारक माना जाता है इसलिए इसे एक व्याधि कीय सामाजिक तथ्य माना जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है।
सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का तात्पर्य श्रमिक वर्ग की जीत से है। इस वर्ग का उल्लेख कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं ‘वर्ग संघर्ष’ के सिद्धान्त का उल्लेख करते समय किया है।
दुर्खीम ने अपनी पुस्तक ‘समाज में श्रम विभाजन’ (The Division of Labour in Society) में श्रम विभाजन का सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। दुर्खीम से पहले एडमस्मिथ, स्पेंसर तथा जॉनस्टुअर्टमिल जैसे विद्वानों ने आर्थिक आधार पर श्रम विभाजन की विवेचना की है। दुर्खीम का कहना है कि श्रम विभाजन की व्याख्या समाज की दशा पर निर्भर है। 19 वीं शताब्दी का समाज ऐसा था जिसमें आधुनिक उद्योग का जन्म हो चुका था। यह उद्योग अपने विकास के दौर में धीरे-धीरे निश्चित रूप से शक्तिशाली मशीनों को अपने अन्दर समा लेता था। ऐसे उद्योग में ज्याद पूंजी का निवेश भी होता था। उत्पादन की मात्रा विशाल होती थी और इन सब शक्तियों के परिणाम स्वरूप समाज में अत्यधिक श्रम विभाजन हो जाता है और प्रत्येक धन्धे में विशिष्टीकरण आ जाता है।
श्रम विभाजन के कारक
दुर्खीम श्रम विभाजन को एक सामाजिक घटना मानते है जो प्रत्येक युग में सभी समाजों की आवश्यक विशेषता रही है। प्राचीन समाजों में श्रमविभाजन का अधार आर्थिक न होकर पूर्णत: सामाजिक ही था उस समय उत्पादन केवल व्यक्तिगत आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए किया जाता था
कारक मुख्यत: तीन है :-
1. जनसंख्या का आकार:- समाज में जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रहती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही समाज के आकार में वृद्धि होती है जब कभी भी समाज का आकार बढ़ता है तब व्यक्तियों की आवश्यकताएं बढ़ने लगती है यही दशा श्रम विभाजन को प्रोत्साहित करने वाला मुख्य कारक बन जाता है।
2. भौतिक घनत्व: भौतिक घनत्व से दुर्खीम का तात्पर्य जनसंख्या के उस घनत्व से है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है किसी समाज में जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तब वहां जनसंख्या का भौतिक घनत्व भी बढ़ने लगता है इसी के साथ ही व्यक्तियों की आवश्यकताओं में वृद्धि होती जाती है।
3. नैतिक घनत्व:- दुर्खीम का विचार है जब संचार के साधनों में वृद्धि होने से व्यक्तियों तथा समूहों के संबंधों में घनिष्ठता उत्पन्न होने लगती है तब इसे नैतिक घनत्व में होने वाली वृद्धि मानना चाहिए। स्पष्ट है कि व्यक्तियों के अन्तर संबंधों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को ही दुर्खीम ने समाज में उत्पन्न होने वाली नयी नैतिकता के रूप में स्वीकार किया तथा इसे श्रमविभाजन को प्रोत्साहन देने वाले एक प्रमुख सामाजिक कारक के रूप में प्रस्तुत किया।
1. विशेषीकरण:-श्रम विभाजन के फलस्वरूप श्रम का विशेषीकरण हुआ है क्योंकि श्रम विभाजन के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कार्य करता है उस कार्य में विशेषज्ञ बनतो जाता है।
2. व्यक्तिवादः श्रम विभाजन ने व्यक्तिवादी भावनाओं को पनपाया है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के फलस्वरूप व्यक्तिगत भिन्नताएं बढ़ती जाती है; व्यक्तियों के अलग-अलग कार्य, अनुभव तथा व्यक्तित्व होते है श्रम विभाजन ने उसे दूसरो के ऊपर निर्भर बनाकर दूसरी के लिए सोचने को मजबूर कर दिया है श्रम विभाजनके कारण सामाजिक कल्याण कार्यों में उसका योगदान बढ़ गया है।
3. गतिशीलधारणाः– दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन एक गतिशील धारणा है और उसमें प्रगति के तत्व छिपे रहते है क्योंकि श्रम विभाजन के फलस्वरूप विशेषीकरण होता है
4. समाज को विभिन्न स्वार्थ समूहों में विभाजितः – श्रम विभाजन समाज को विभिन्न स्वार्थ समूहों में विभाजित कर देता है और कुछ सीमा तक आपसी मतभेद भी उत्पन्न कर देता है।
5. समाज के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर:- श्रम विभाजन समाज को विभिन्न सदस्यों और समूहों को एक दूसरे पर निर्भर कर देता है इस पारस्परिक निर्भरता के कारण व्यक्तिवाद की भावना है कटुरूप में पनप नहीं पाती है। श्रम विभाजन के कारण प्रत्येक अपनेव्यक्ति पर इस प्रकार का एक नैतिक दबाव होता है।
6. श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण व्यक्तिमत्तगुण तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का महत्व भी बढ़ गया है।
7. श्रम विभाजन ने समाज को अनेक स्वार्थ समूहों तथा व्यवसायिक समूहों में बांट दिया है।8. श्रम विभाजन की मुख्य उपयोगिता यह है कि इसे अधिक धन तथा उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अभिलाषा की पूर्ति के 1 साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
निष्कर्ष
Bhartiya Sarokar पर आपका स्वागत है इस पोस्ट के माध्यम से हमारे द्वारा देखिए से दुर्खीम संबंधित पूरी जानकारी उनके सिद्धांत उनके से संबंधित पूरी जानकारी दे चुके हैं और आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो अधिक से अधिक शेयर करें।
FAQ
Q. दुर्खीम का सिद्धांत क्या है?
A. दुर्खीम का यह सिद्धान्त धार्मिक व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाता है।
Q. दुर्खीम के दो योगदान क्या है?
A. समाजशास्त्र को एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान बनाने का प्रयास किया और रहस्यवाद, अधिप्राकृतिकवाद एवं परंपरावाद का विरोध करते हुए सामूहिकता और सामजिक मूल्यों को सामाजिक जीवन का वास्तविक आधार बताया।